
नए साल में आने के बाद भी समय है कि बदलने का नाम नहीं ले रहा। अपने आस-पास जिस तेजी से लोगों को, अपने जानने वालों को, अपने क़रीबी जनों को कोरोना के संकट से जूझते और बहुतों को हारते देख रहे हैं, वह शायद हम सभी की ज़िंदगियों का अभूतपूर्व अनुभव है। हमारी स्वास्थ्य-सेवाओं की दिन-प्रतिदिन चरमराती हालत, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, आक्सीजन की भारी किल्लत, महत्वपूर्ण दवाइयों की कालाबाज़ारी, इन सबने स्थिति को और भी ज़्यादा भयावह बना दिया है। लोग अपने प्रिय जनों के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर औसतन 3 में से एक पोस्ट इन्हीं मदद की गुहारों से भरे हैं। तमाम छोटे-बड़े शहरों से आने वाले शमशान घाटों के आँकड़े दिल दहलाने वाले हैं, लोग अपने संबंधियों को आखिरी विदा देने के लिए भी क़तारों में लगे रहने को विवश हैं।
दिन-प्रतिदिन बीमारी के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए सरकारें अपने-अपने स्तर पर निर्णय ले रही हैं। शहरों को बंद कर दिया जा रहा है, आवागमन रोका जा रहा है, दूसरे राज्यों से युद्ध स्तर पर आक्सीजन, दवाइयां मुहैया कराई जा रहीं हैं। हज़ारों की संख्या में प्रवासी मज़दूर अपने-अपने घरों को लौटने के लिए विवश हैं। न जाने कितने बेघर हो कर, भूख और बीमारी से बचने के लिए वापस जा रहे हैं।
सब ओर भीषण शोक की, भय की स्थिति है। ऐसा लगता है मानो समय की सूई ही शोक की इस त्रासद स्थिति पर आकर रुक गई है। ऐसे में वो लोग जो अब तक शायद सुरक्षित हैं, या जिन्हें इतनी सुविधाएं हैं कि अपने सुरक्षित घरों में रह कर स्थिति को सिर्फ देख रहे हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए या कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए भी या नहीं ? और क्या इस प्रश्न पर सोचा जाना भी चाहिए या नहीं?
मानते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, ज़िंदगी थमने का नाम नहीं लेती। लोग काम करेंगे ही, जिनके पास संसाधन हैं, वो अपनी छुट्टियाँ मनाने इग्ज़ाटिक लोकैशन (exotic locations) पर जाएंगे ही, यूट्यूब से अपनी आजीविका चलाने वाले अपनी मामूली-से-मामूली, निहायती मन्डेन (mundane) दिनचर्या अपलोड करेंगे ही, सोशल मीडिया-इंस्टाग्राम,फेसबुक या व्हाट्स एप के स्टैटस पर अपने बनाए गए खानों की, अपने लगाए पौधों की, अपने मनाए गए त्योहारों की तस्वीरें डालेंगे ही। क्योंकि जैसा कि कहा, ज़िंदगी तो रुकेगी नहीं। और सबसे बड़ी वजह यह कि यह सब जो कुछ भी घट रहा है, वह हमारे साथ तो नहीं घट रहा है न, लोग जिनके मरने की, जिनके संक्रमित हो जाने की खबरें आती हैं वो कोई भी हो सकता है, वो ‘हम’ तो नहीं हैं न।
ऐसा लगता है कि लोग और उनकी परेशानियाँ बस खबरें बन कर रहीं गई हैं। ऐसी खबर जिसे चाय की चुस्की के साथ अपने खाने की मेज़ पर अख़बार में पढ़ा जाता है और जिस तरह से रद्दी में अख़बार चला जाता है, ख़बर भी, और इन ख़बरों के लोग भी स्मृति से, अपनी संवेदना से परे हटा दिए जाते हैं। और हम उठ कर अपने काम में लग जाते हैं। सोच का छटांक बराबर क़तरा भी किसी और पर, किसी और के कष्टों पर क्यों ज़ाया किया जाए। अरे! उतनी ही देर में थाली में परोसे गए खाने की तस्वीर न ले ली जाएगी, या अपना कोई सेल्फ़ी ही नहीं खींच ली जाएगी क्या?
हंसी आती है और गहरा क्षोभ भी होता है। नहीं पता, नहीं पता कि हमारी आधुनिक ज़िंदगी किस दिशा में बढ़ रही है? ये जो अपने खुद के बनाए गए बबल हैं, सुरक्षा के, सुविधाओं के वो सारे घेरे, जहां व्यक्ति सिर्फ स्वयं से प्रेम करता है, अपनी कल्पनाओं में मग्न रहता है, वह क्या आज के समय की आवश्यकता है या आज के समय का कड़वा यथार्थ ? मनुष्य जाति क्या अब संवेदनशील नहीं रही या हमारे 23 जोड़ों वाले क्रोमज़ोम ही अब संवेदना के जीन के बिना बन रहे हैं? बहरहाल, वजह चाहे जो भी हो, हम मनुष्यों की हरकतें तो यही साबित करती हैं कि हम सामूहिक शोक की इस घड़ी में भी, अपनी ही खयाली दुनियां के सुखों के फूहड़ प्रदर्शन में व्यस्त हैं।
पर हम क्या चाहते हैं? कि हर इंसान वाकई इंसान बन जाए? या कोई सोशल ऐक्टिविस्ट बन कर सड़कों पर निकल जाए या अस्पतालों में जा-जाकर मरीजों की मदद करे, या और कुछ नहीं तो उनके सगे-संबंधियों को ही सांत्वना देने लगे? हर घर क्या किसी प्रवासी मज़दूर के, उसके परिवार के भरण-पोषण का जिम्मा उठा ले, और वह भी सिर्फ इस नाम पर कि उनके पास इन ग़रीब मज़दूरों की अपेक्षा ज़्यादा संसाधन हैं? आखिर लोगों से, अदना-सी ज़िंदगी जीने वाले लोगों से, हमें इतनी महान अपेक्षाएं ही क्यों हैं ? ऐसा सब करने से क्या ये जो स्थिति है, ये जो भय के हालात हैं, वह बदल जाएंगे?
नहीं.. कतई नहीं। कुछ नहीं बदलेगा, लोग बीमार होंगें ही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आधार पर मरेंगे ही, ग़रीब और ग़रीब ही होंगे, भले ही अरबपति इन सालों में और भी अरबों की कमाई करते चलें, जिनकी ज़िंदगी प्रभावित होनी है, वो होगी ही, कहने का अर्थ कि कुछ भी बदलेगा नहीं। कुछ भी नहीं।
फिर? फिर , इस सोच-विचार की आवश्यकता? क्यों न ज़िंदगी को उसकी स्वाभाविक गति से चलने दिया जाए.. नदी को धारा के विपरीत मोड़ने की ज़रूरत ही क्यों ?
पर.. ज़रूरत है.. ज़रूरत तो बिल्कुल है। क्या हम चाहते हैं कि इतिहास जब इस समय को, इन वर्षों को, अपने पन्नों में दर्ज़ करेगा तो, हमारी, हम सुविधा-सम्पन्न वर्गों की असंवेदनशीलता पर, हमारी तटस्थता पर हँसकर इस गुजर गई सदी पर लानत भेजेगा? और इतिहास की छोड़ें, वह तो दूर की बात है। क्या हम यह चाहते हैं कि जिस नीम बेहोशी में हम अपनी चेतनाओं को, अपनी मानवीयता को बंद कर के जी रहे हैं, संभवतः होश आने पर खुद पर ही शर्म करें?
मानते हैं कि कुछ बहुत आंदोलनकारी या युगांतरकारी क़ारनामे अभी नहीं किए जा सकते पर, संवेदनशील बने रहने में कोई बहुत बड़ा खर्च तो नहीं आता? कोई नहीं चाह रहा कि आप साधन-सम्पन्न हैं तो बड़ी रकम दान में दे दें, पर लोगों के प्रति , उनके दुखों के प्रति सहानुभूति अनुभव करने में तो अपनी तरफ से कुछ नहीं लगता? पर फिर भी हम हैं कि अपने ‘बबल’ में लिप्त हैं, हमारे तबीयत की रंगीनियाँ हैं कि कम होने का नाम नहीं लेतीं। क्या अब साधारण लोग भी अपने-आप को फिल्म-स्टार समझने लगे हैं? मतलब कि एक ऐसा निस्संग वर्ग जो अपनी ही रंगीनियों में डूबा हुआ, खुद को हद से अधिक आकर्षक बना लेने की चाह में दिन-रात कसरतों में लगा रहता है।
अपनी थोड़ी-सी संवेदनशीलता ऐसे समय में, अगर हमारे हिस्से से निकले तो बहुत बड़े परिवर्तन तो नहीं आएंगे, पर शायद जो पीड़ित हैं, जिनके सरों से इस बीमारी ने साया छीन लिया है, या जिनकी दो वक़्त की रोटी का साधन समाप्त हो गया है, उनके जलते हृदय पर थोड़ी तो ठंडक पहुंचेगी, और कम-से-कम वो हमारी सहानुभूति पाकर इस पूरे संघर्ष में, इस पूरी वेदना में शायद कुछ क्षणों के लिए तो अकेला न महसूस कर पाएंगे ।
क्यों आज किसी का व्यक्तिगत शोक, सामूहिक शोक नहीं बन सकता ? क्यों इस बीमारी से जूझ रहे लोग, उनके परिवार अपने दुख में हर किसी का साथ नहीं पा सकते? साथ देने का मतलब यह तो नहीं कि हम स्वर मिला कर रोने लगें, पर साथ देने का अर्थ, इस समय तो महज़ इस बात से सार्थक हो जाएगा कि अपनी सुविधाओं का, अपने सुख का निर्लज्ज सार्वजनिक प्रदर्शन तो न करें। फिल्म स्टार मालदीव में छुट्टियाँ बिताते हुए सोशल मीडिया पर अपने सुख के क्षणों को जिन लोगों से साझा कर रहे होते हैं, क्या पता उनमें से कितनों के घर ठीक उसी क्षण कोई चल बसा हो सकता है, या कोई आक्सीजन के सिलेंडर के लिए सड़कों पर मारा-मार फिर रहा हो। या, अच्छा खाना अगर आज हमें नसीब हुआ है तो बजाय उस ऊपर वाले को शुक्रिया करने के उसे अपने फेसबुक या व्हाट्स एप पर डाल कर अपने असंवेदनशीलता का तो प्रदर्शन न करें। क्योंकि क्या पता जिस क्षण हम वो तस्वीर अपलोड कर रहे होंगे, कोई बेसहारा मज़दूर इस लॉक डाउन में शायद कई दिनों से काम पर न जाने की वजह से खुद भी भूखा होगा और उसके छोटे बच्चे भी बिना खाए सोये होंगे।
ऐसे में, बस चाहिए तो सिर्फ थोड़ी सी मानवता। किसी के दुखों को अनुभूत कर पाने की संवेदनशीलता। इससे कुछ होगा नहीं, पर यकीन मानें हम इंसान बने रहेंगे, आगे चल कर अपने पर शायद शर्म करने की गुंजायेश भी कम हो जाएगी।


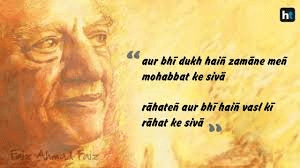




Leave a reply to Aditi Bhardwaj Cancel reply