
अचानक ही आ गए थे। कभी सोचा हो या चाहा हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं । बहन के घर पर देखा करती थी, तो बस एक दर्शक की तरह। न कोई जुड़ाव न कोई लगाव। नहीं समझ पाती थी, कि क्यों उनका पूरा परिवार इनके पीछे दीवाना था। अक्सर घर पर इस दीवानगी का मजाक उड़ाया जाता तो कई दफा मैं भी शामिल रहती। पर जब एक दिन बहन ने मुझे भी एक जोड़ा इन परिंदों का जन्मदिन के तोहफे में दे दिया तो , पिंजड़ा थामे खुशी के चरम पर पहुँच कर शायद मैंने ही तस्वीर खिंचवाई थी।
और बस एक शाम बिना किसी योजना, बिना किसी मंसूबे के Budgies या Australian Parakeets की जोड़ी मेरे घर का हिस्सा बन गई। पसंद के रंग थे, एक हल्के नीले रंग का , जिसे दूर से देखो तो आसमान का एक टुकड़ा लगता था, और दूसरा थोड़ा हरा ,थोड़ा पीला को मिलकर बनाया गया रंग जो कभी तो एकदम पीला लगता तो कभी हल्का हरा। छोटे से सफेद पिंजरे में दुकानदार ने झूले, खाने के रंगीन बर्तन, पानी के मर्तबान के साथ दिया था। उस सफेद छोटे पिंजरे में इन दो परिंदों को या यूं कह लें पक्षी-शावकों को देखना किसी चित्रकार की पेंटिंग देखने जैसा था।

नए घर में एक पूरा दिन ये सहमे हुए थे। मुझे अपने पास आता देख घबरा कर पिंजरे के किसी कोने में छुप जाते। न खाने को हाथ लगाते, न पानी को। एक पूरा दिन बीत जाने पर कौतूहल ने चिंता का रूप लिया। अगर इसी तरह भूखे-प्यासे अनसन पर बैठे-बैठे प्राण दे दिए तो? बहन से पूछा, फिर गूगल पर तमाम जानकारियाँ इकट्ठा कीं , तब जाकर पता चला कि नए परिवेश में अभ्यस्त होने में हम इंसानों की तरह इन परिंदों को भी वक़्त लगता है। मन शांत हुआ, पर दिल में कसक थी कि बेचारे न जाने कितने घंटे से भूखे हैं। अगला दिन हुआ, तो ज़िंदगी की तरह ही इनकी भूख-प्यास भी पटरी पर आ गई। हालांकि अभी प्रगति इतनी ही थी कि मेरे पिंजरे से दूर जाने पर ही दाने की कटोरी पर बैठते और मेरी आहट पाते ही फिर वैरागी की तरह एक कोने में समाधिस्थ हो जाते।
जितनी जानकारी इकट्ठी की जा सकती थी, जितने तरह के संसाधन इनके लिए जुटाए जा सकते थे, वह सब लगभग कर लिया। इसी जद्दोज़हद में यह भी पता चला कि कैद हैं तो क्या हुआ, जगह तो ज़्यादा चाहिए- ताकि सीमित ही सही, पर उड़ान तो ले सकें, पंखों को फैला कर कसरत तो कर सकें। और इन सबके लिए पिंजरे को बड़ा करने की आवश्यकता थी, सो फिर क्या था, नीले ही रंग का एक बड़ा पिंजरा इनका नया घर हो गया। तरह-तरह के रंगीन झूले, समय व्यतीत करने के लिए खिलौने यह सब उस घर में लटकाए गए। पिंजरा, पिंजरा न लग कर मानो मेरा अपना घर हो गया, जिसके हर एक कोने को सजा-धजा कर रखना एक अच्छे घर की, अपने व्यक्तिगत स्पेस की अदद ज़रूरत बन गया।

अब मसला नाम का था। जन्म के समय इनके वालदैन ने इनका क्या नाम रखा था, वह तो ठीक-ठीक पता कर पाना मुश्किल था, इसलिए नाम देने की नई जिम्मेदारी भी अपने ही सर पड़ी। और नाम देना जरूरी था, कारण कि सिर्फ जातिवाचक नाम से पुकारते रहना भी सही नहीं था। ‘चिड़िया’ खाना खा लो, या ‘चिड़िया’ पाने पी लो, कहना थोड़ा तो अपमानजनक होता। पर इस के अलावा शायद एक स्वार्थी कारण भी था, लगा कि नामकरण कर देने से, अपने नाम देने वाले को तो कम से कम पहचाना करेंगे । मेरी एक पुकार पर दौड़े चले आएंगे, दूसरों के सामने अपने इस कारनामे का प्रदर्शन और फिर प्रशंसा का लोभ भी था। इसलिए नाम रखना तो जरूरी था, चाहे शेक्सपियर लाख कहते रहें ““What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.”
रंगों के हिसाब से नीलू-पीलू, रखा जाना सरल था, पर ये भी कोई नाम हुए। ऐसा लग रहा है मानो परिंदे न हुए, कुपोषण के शिकार मरियल टांगों से चलते हुए दो बच्चे आ कर खड़े हो गए हों। नाम तो भई , कुछ ऐसा हो जो अलग भी हो, और जिसे सुन कर लगे कि माडर्निटी और संस्कृति का संगम हो। ठीक कुछ ऐसा जैसा आज कल के नए जन्मे बच्चों का नाम उनके माता-पिता उत्तर-वैदिक कालों से खुदाई कर के लाते हैं और ऐसा लगता है , मानो ‘वेदों की ओर लौटो’ की कहावत को कम से कम नाम के तौर पर तो सिद्ध कर ही लिया जाए। खैर, मैं वेदों की इतनी बड़ी उदगाता तो नहीं , पर Netflix के सुर अच्छे से पता हैं -तो एक को थोड़ा मॉडर्न बनाते हुए ‘पाब्लो’ कर दिया और दूसरे को लोक संस्कृति से जोड़ कर पक्षी का ही पर्यायवाची ‘परबा’ कर दिया। अटपटे थे, पर यकीन माने जब कभी इस नाम को लेती तो दोनों मेरी ही ओर देखते, पर शायद अपने उत्साह में यह भूल जाती कि ये पक्षी आवाज की दिशा में देख रहे हैं, अगर में इनकी जगह प्याज या टमाटर भी कहती तो देखते ही। बहरहाल, नाम की समस्या, निपट गई थी और मैं अपनी खुश-फहमी में विभोर थी।

दिन बीतते गए। मेरी अपनी व्यस्तता में इनके रहने से कोई विशेष व्यवधान हुआ हो ऐसा नहीं। बस सुबह में दाना पानी दे देने के बाद, इनसे छुट्टी मिल जाती। फिर ये भी अपने खाने और खेलने में व्यस्त रहते। एक छोटे पिंजरे में करने को बहुत कुछ था भी नहीं। इसलिए दिन के समय जब झपकी लेते इन्हें देखती तो लगता कि इंसान की तरह ही ये परिंदे भी, कुछ काम न होने की स्थिति में बोरियत महसूस करते हैं। घर के बाहर बिलकुल जंगल है। नीम के घने पेड़ों पर असंख्य पक्षी दिन-रात चहचहाते हैं। प्रकृति के ऐसे आँगन में अपने इन परिंदों को भी मैं कुछ देर नियमित रूप से रखने लगी। सुबह और शाम के वक़्त जब सूरज की किरणें तीखी न होती तब पिंजरा बाहर बालकनी में डाल देना रोज़ का काम बन गया। इन्हें भी जंगल और चिड़ियों का शोर मदमस्त कर देता। कमरे में जहां सारा वक़्त खाने की कटोरियों के इर्द-गिर्द बीतता, वहीं बाहर बालकनी में खाने की सुध-बुध भूल कर बस पिंजरे की दीवारों से लटक लटक कर शोर मचाते रहते। आस-पास के पेड़ों पर बैठे परिंदे भी मानो इन्हें खुश करने के लिए और शोर मचाते। कभी-कभी वाकई लगता किअसल के चिड़ियाखाने में रहने लगी हूँ।



पर कुछ भी हो, इन निरीह , बेज़ुबान परिंदों ने अपनी खामोशी से भी बहुत कुछ सिखला दिया था। सूरज की रोशनी के साथ उठना, शाम के साथ अपनी गति कम कर लेना, कम से कम में भी खुश रहना। कई दफे मन में खयाल भी आया कि इस तरह पंछी को पिंजड़े में क़ैद कर के पालना कहाँ तक सही है? जब हम इंसानों को अपनी आज़ादी इतनी पसंद है , तो ये कैसे मुमकिन है कि इन परिंदों को चाहे एक बड़े पिंजड़े में ही क्यों न रख दिया हो, अच्छा लगेगा? पिंजड़ा तो पिंजड़ा है, क़ैद तो क़ैद है। फिर चाहे वह सोने का बना पिंजड़ा ही क्यूँ न हो। पक्षी को तो आसमानों की उड़ान भरने के लिए ही पंख दिये गए हैं। अपने आकर्षण और मनोरंजन के लिए उनके उड़ान को पिंजड़े में क़ैद कर देना कहाँ तक नैतिक है? इसलिए मन बहुत सारी दुविधाओं में एक साथ रहता था। जहां इन्हें शोर मचाता, करतब करते देख खुश होती तो, वहीं सामने के पेड़ों पे बैठी चिड़ियों को देख कर, उनकी स्वच्छंदता को देखकर मन में अपराध-बोध भी होता।
बहरहाल, दिल कभी इतना बड़ा न कर पायी कि इन्हें उड़ा दूँ। ये परिंदे इतने छोटे थे कि बाहर उड़ते चील और बाज़ मिनटों में इन्हें अपना शिकार बना लेते। शायद यही सब दिलासा देकर के मैं इन्हें अपने पास रहने देने की दलीलें अपने मन को दिया करती। पर शायद हमारा मन जिस बात से डरता है, कभी-कभी उसके सच हो जाने की स्थिति भी आ जाती है।

प्रायः शाम को क़रीब 6 बजे के आस पास मैं पिंजड़ा उठा कर बालकनी में रखा करती थी, पर शायद उस दिन बारिश की वजह से दोपहर से ही मौसम सुहाना लगने लगा था। जी आया कि अंदर की उमस से अच्छा इन्हें बाहर की ताज़ी हवा में रख दूँ, सो पिंजड़ा उठा कर बाहर रख दिया। इन्हें खुश-खेलता देख कर प्रसन्न मन से अंदर आ कर अपने काम में लगी। बस, इतना ही हुआ था। और जब थोड़े देर बाद बाहर आई तो देखती हूँ, कि हर जगह इनके पंख बिखरे हुए हैं। मुझे लगा, वैसे भी इन्हें हर वक़्त अपना पंख सहलाने की आदत होती है तो शायद वही है, पर जब आँखें ज़मीन से उठ कर पिंजड़े की तरफ गयी, तो मुंह से चीख निकल गयी। बस एक वो मंज़र है, और एक आज का दिन। खौफ खत्म नहीं हो पा रहा। पिंजड़े में शायद किसी बाज़ या चील या किसी और शिकारी चिड़िया ने इन पर हमला कर दिया था , और ये दोनों भी पूरे संघर्ष के बाद ही शायद थक-हार कर एक कोने में मृत पड़ी हुई थीं। डेढ़ महीनों के इनके साथ का यह अंत हुआ।
कितना रोयी, चीखी-चिल्लाई इसका तो ज़िक्र ही क्या, बस अनहोनी के बाद जिस तरह की मन:स्थिति हो जाती है, जहां हम एकबारगी भरोसा नहीं कर पाते कि अभी-अभी जो घटा है, क्या वह सच में हुआ है, या कोई बुरा सपना देख रहे हैं। अपने आप को बहुत झकझोरा कि क्या पता नींद में होंऊं, और यह सब कुछ नहीं हुआ हो, सब महज़ सपना हो। पर ऐसा भी कभी होता है। अच्छी चीज़ें सपना भी हों, बुरी चीज़ें नहीं, ज़िंदगी ने इतना तो सिखला ही दिया है। तो मेरे इन परिंदों की ज़िंदगी का ऐसा भयानक अंत वाकई एक सच्चाई थी, जिसे चुपचाप स्वीकार करना था।
कितनी बार हमें लगता है कि काश हम ज़िंदगी को रिवाइंड कर के, कुछ-कुछ जगहों पर जाकर , किसी चीज़, या किसी काम को सही कर पाते। ऐसा ही लग रहा था कि क्या ही अच्छा होता जो, मैं उस दिन पिंजड़ा उठा कर बाहर न ले गयी होती, या बारिश के बदले हर दिन वाली गर्मी ही हुई होती। पर जैसा कि कहते हैं, अनहोनी को कौन टाल सकता है। रोज़ ही तो बाहर रखा करती थी, फिर उसी दिन ऐसा हादसा होना तो यही साबित करता है कि बकरे की अम्मा कब तक ख़ैर मनाएगी। उस दिन न सही, शायद फिर किसी दिन हो जाता, पर बाहर रखना असुरक्षित था, इतनी समझ तो मुझे उन दो परिंदों को गंवा कर ही आई।
ख़ैर, जिनकी मौत ठीक से न हुई, उन्हें अंतिम विदा तो अच्छी तरह से मिलनी चाहिए थी। सामने के पार्क में, अपने इन प्यारे और अनोखे पंछियों को जाकर मिट्टी में दफना आई, अगरबत्ती की सुगंध, फूलों और घास से मानो इनका एक मज़ार ही बना दिया। इस कोरोना के भीषण समय में, जहां लोगों के प्रियजनों को शमशान घाटों के किनारे नसीब नहीं हो पा रहे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में गंगा में लाशें बहा दी जा रही हैं, वहाँ, मेरे इन दो पंछियों को अंतिम विदा देना कितना सार्थक है, इस पर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। पर मेरे आसरे में रहने वाले ये दो बेज़ुबान जीव, मुझसे इतनी तो अपेक्षा रखते ही थे कि मैं उन्हें यूं ही किसी कचड़े के ढेर में न फेंक दूँ।


बहरहाल, आलम यह है कि, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। घर पर पड़े सूने पिंजरे को देखते रहना, उन परिंदों की मौत से भी ज़्यादा दुखदायी था। अंत में यही सलाह हुई कि उस हादसे से उभर कर फिर से दिल बड़ा कर के नए परिंदों से वह सूना पिंजड़ा भर लूँ, ताकि विरह के गीत लिखने से बचूँ और मेरे क़रीबियों को ज़बरदस्ती लिखे गए गीतों को पढ़ना न पड़े। तो सोच और समझ की क्षमता से परे जाकर, मैंने फिर से कुछ नए परिंदों को उस पिंजड़े में जगह दे दी है। क़ैद कर के रखने से भी ज़्यादा जरूरी अब शायद उनकी प्राण रक्षा हो गयी है, इसलिए इस पक्षी-रक्षा के भाव से प्रेरित हो कर सूने पिंजड़े को भर लिया गया है।और जैसे दूध का जला छांछ भी फूँक-फूँक कर पीता है, मैंने भी इन परिंदों को खुली बालकनी में अकेला न छोड़ने की क़सम खा ली है।

फिलहाल तो ये नए हैं, इतना लगाव नहीं है इनसे। पर अपने पुराने परिंदों के बिछुड़ने का ग़म अब भी सालता है। इनके आ जाने के बाद भी, शायद उस ज़ख्म को भरने में अभी वक़्त लगे। आखिर इंसान हैं हम, इतनी आसानी से सब कुछ भुला कर आगे बढ़ा नहीं जाता। पर जो छूट गए हैं, उनके अच्छे पलों का जश्न मनाना कहाँ मना है और उजड़े घर को बसाना कहाँ गुनाह है। वो हरिवंशराय बच्चन कहते हैं न:
“क्या हवाएँ थीं कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना,
कुछ न आया काम तेरा शोर करना, गुल मचाना,
नाश की उन शक्तियों के साथ चलता ज़ोर किसका,
किन्तु ऐ निर्माण के प्रतिनिधि, तुझे होगा बताना,
जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से,
पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है?
है अँधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है?

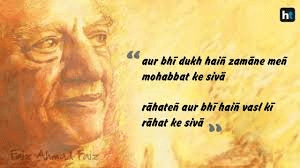




Leave a comment