बीच बहस में यूं ही जब
लगे कि सब हैं खड़े एक तरफ
हैं सबकी धारणायेँ एक और
सबके सुर भीं हैं एक
तब क्या बचते हैं खुद को अलग रख पाने के उपाय?
शायद बहस का उत्तर एक और बहस,
तर्क का समाधान एक और तर्क से
या फिर होठों पर चुप लगाकर करना
आँखों से केवल अपना विरोध
दिल-ही-दिल में सुलगते रहने के बजाय।
पूछा है स्वयं से कई बार कि
क्यूँ नहीं चलता है मन बेकाबू भीड़ के साथ?
क्यूँ जो तमाम के लिए है अच्छा
सहज ही मान लिया गया है सब के लिए अच्छा?
थोड़ी मुख़्तलिफ़ क्यूँ न हो हमारी राय।
सोचा है कभी, इस तर्कहीन स्वीकार के परिणाम
या इस निराधार आस्था के अंजाम ?
है ख़तरा कि भेड़ों में तब्दील हो जाएंगे इंसान
जो कभी धर्म तो कभी सत्ता के हाथों
शहादतें देने को होंगे विवश और निरुपाय।

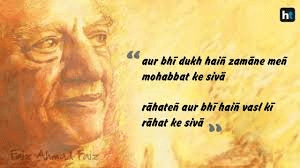




Leave a comment